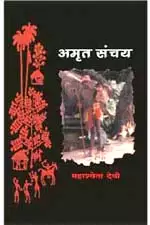|
ऐतिहासिक >> अमृत संचय अमृत संचयमहाश्वेता देवी
|
112 पाठक हैं |
|||||||
‘अमृत संचय’ 1857 के विद्रोह के समय बंगाल की अवस्था का चित्रण करती है...
Amrit Sanchaya - A hindi book by Mahasweta Devi
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
आदिवासी जीवन की प्रामाणिक जानकार के नाते ख्यात लेखिका महाश्वेता देवी ने इतिहास को भी अपने लेखन का विषय बनाया है। पहले उपन्यास झाँसी की रानी, जली थी अग्निशिखा से लेकर प्रस्तुत उपन्यास अमृत संचय तक इस बात के गवाह हैं।
यह उपन्यास सन् 1857 से थोड़ा पहले शुरू होता है जब सांगठनिक दृष्टि से देश कमज़ोर था। सभी अपने-आप में मगन, अलग-अलग समूहों, खेमों और राज्यों में विभाजित। 1857 के विद्रोह में बंगाल ने किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं निभाई थी। उधर संथाल में अंग्रेज़ी सत्ता के विरूद्ध बग़ावत, नील-कर को लेकर असंतोष और अपेक्षित वेतन न मिलने के कारण सेना भी असंतुष्ट थी। उपन्यास इसी संधिस्थल से आरंभ होता है और तैंतीस वर्षों बाद उस बिंदु पर ख़त्म होता है, जहां भारतीय जनमानस के चेहरे और विन्यास में बदलाव नजर आने लगा था। गहन खोज और अध्ययन, परिश्रम का प्रतिफल यह उपन्यास तत्कालीन समय की राजनीति, इतिहास, आम जन के स्वभाव-चरित्र, रंग-ढंग, रिवाज-संस्कार को प्रामाणिक तौर पर हमारे सामने लाता है। हालाँकि देशी-विदेशी सौ चरित्रों को समेटना मुश्किल काम है, पर महाश्वेता देवी ने अपनी विलक्षण बुद्धि और शैली के बूते इसे संभव कर दिखाया है। लेखिका की पहचान रही उन तमाम खू़बियों को समेटे यह बंगला का प्रमुख उपन्यास माना जाता है जिसमें विपरीत स्थितियों में भी जीवन के प्रति ललक है और संघर्ष की आतुरता शेष है।
यह उपन्यास सन् 1857 से थोड़ा पहले शुरू होता है जब सांगठनिक दृष्टि से देश कमज़ोर था। सभी अपने-आप में मगन, अलग-अलग समूहों, खेमों और राज्यों में विभाजित। 1857 के विद्रोह में बंगाल ने किसी भी प्रकार की हिस्सेदारी नहीं निभाई थी। उधर संथाल में अंग्रेज़ी सत्ता के विरूद्ध बग़ावत, नील-कर को लेकर असंतोष और अपेक्षित वेतन न मिलने के कारण सेना भी असंतुष्ट थी। उपन्यास इसी संधिस्थल से आरंभ होता है और तैंतीस वर्षों बाद उस बिंदु पर ख़त्म होता है, जहां भारतीय जनमानस के चेहरे और विन्यास में बदलाव नजर आने लगा था। गहन खोज और अध्ययन, परिश्रम का प्रतिफल यह उपन्यास तत्कालीन समय की राजनीति, इतिहास, आम जन के स्वभाव-चरित्र, रंग-ढंग, रिवाज-संस्कार को प्रामाणिक तौर पर हमारे सामने लाता है। हालाँकि देशी-विदेशी सौ चरित्रों को समेटना मुश्किल काम है, पर महाश्वेता देवी ने अपनी विलक्षण बुद्धि और शैली के बूते इसे संभव कर दिखाया है। लेखिका की पहचान रही उन तमाम खू़बियों को समेटे यह बंगला का प्रमुख उपन्यास माना जाता है जिसमें विपरीत स्थितियों में भी जीवन के प्रति ललक है और संघर्ष की आतुरता शेष है।
निवेदन
‘अमृत संचय’ उपन्यास जहाँ से शुरू होता है, उस ज़माने में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। डलहौजी ने Doctrin of Lapse नीति, नए सिरे से जारी कर दी। सन् 1856 में अयोध्या, अंग्रेज-शासित भारत में शामिल कर लिया गया। इसलिए वहाँ के जमींदार और भू-मालिकों से लेकर विपुल संख्यक किसान तक सभी विक्षुब्ध हो उठे। सन् 1855-56 में संथाल विद्रोह छिड़ गया। बंगाल और बिहार में नील-कर के खिलाफ असंतोष का धुआँ उठने लगा। इधर फौज और घुड़सवार सेना अपनी तनख्वाह और तरक्की वगैरह में नाइंसाफी को लेकर बेहद नाराज। इसी दौरान छोटे-छोटे भूस्वामी और सरदार, कारोबारी और व्यापारी भी, अपनी-अपनी स्वार्थ-सिद्धि में व्याघात पड़ने की आशंका से आतंकित। शासितों का अपने शासकों पर भरोसा नहीं था, शासक को भी उनका भरोसा अर्जित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
विशाल भारत का सामग्रिक रूप, लगभग लुप्तप्राय। तमाम प्रदेश अलग-अलग द्वीपों में बँटे-बिखरे; आत्मकेंद्रित ! आम इनसान ज्यादातर अपने-अपने में मगन। अशिक्षा और कुसंस्कारों ने उन्हें दास बना डाला था। दूसरी तरफ क्षमता का लोभ, धन-दौलत की प्रचुरता और इन्हीं के बीच हिंदू-मुसलमान और आंग्ल समाज की पँचमेल सभ्यता का शोरगुल। इसी संधिस्थल से यह उपन्यास शुरू होता है। और तैंतीस साल बाद उस बिन्दु पर खत्म होता है, जहाँ भारतीय जनमानस के चेहरे और विन्यास में परिवर्तन का आभास नज़र आने लगा। जहाँ व्यक्ति-चेतना और सोच-विचार में शिक्षा का प्रभाव स्पष्ट आकार लेने लगा था।
सन् सत्तावन में अंग्रेजों की हुकूमत। उन दिनों भारत के दो-तिहाई हिस्सों में जो विराट अभ्युत्थान करवट ले रहा था, उसकी गति-विकृति के बारे में आज भी मतविरोध है। किसी-किसी की राय इसे ‘पहला स्वतंत्रता संग्राम’ या ‘राष्ट्रीय विद्रोह’ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय विरोध, राष्ट्रीय विद्रोह के सुपरिचित लक्षण, इनका अभीष्ट लक्ष्य और संघर्ष के तरीकों में समानता का अभाव था। उन लोगों की नज़र में यह एक ‘आपात घटना’ या ‘Immediate event’ थी।
दूसरी तरफ इसे ‘आपात घटना’ न मानते हुए, कई-कई इतिहासकारों की राय में फौजी विक्षोभ का कारण किसान वर्ग के जीवन में निहित था, जो कर्ज़ से जर्जर और गरीबी की मार से बदहाल थे। इसे ‘Civil rebellion’ नाम देकर, इस विद्रोह को समाज के विभिन्न स्तरों पर छिड़े विभिन्न विक्षोभों के साथ जोड़कर, इनमें एक योगसूत्र क़ायम करने की कोशिश की गई। इन इतिहासकारों का शायद यह खयाल है कि सिपाहियों के उस शोषण की वजह से भारतीय जनमानस में परिचित तजुर्बों की बुनियाद हिल गई और उस दिन से शिक्षित समाज के मन में भी ब्रिटिश शासन के प्रति विद्वेष गहराने लगा। बाद में वही राष्ट्रीय संग्राम की नवीनतम पटभूमि के सृजन का सूत्रधार बना। नील विद्रोह, प्रेस एक्ट और एलबर्ट बिल वगैरह के जरिए प्रत्यक्ष न सही, अप्रत्यक्ष रूप से शायद वही लालसा ही फलीभूत हुई। सन् 1857 के आन्दोलन में बंगालियों की कोई भूमिका क्यों नहीं थी, इस बारे में भी कई-कई मतविरोध हैं। बहरहाल, वजह चाहे जो भी हो, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस ज़माने में बंगाली समुदाय अगर इस विद्रोह में भागीदार होता भी तो अंग्रेज़ी शासन का आकस्मिक अवसान नामुमकिन था और बाद के वक्तों में शिक्षा, शिल्प, ज्ञान साहित्य के क्षेत्र में और स्वस्थ, सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अप्रतिबद्ध वर्ग के तौर पर बंगाल का जबर्दस्त आत्मप्रकाश, भारतीय इतिहास को इस क़दर जटिल, विचित्र और अमोघ नहीं बना पाता।
मैंने उपन्यास में भारतवर्ष के उस संकटकाल और संसूचित नव-चेतना के समय को सफल साबित करने की कोशिश की है। उपन्यास लिखते हुए किसी सुनिश्चित कहानी की ज़रूरत होती है। लेकिन उस कहानी को छोड़ दें, तो उस युग के भारतवर्ष का राजनीतिक-सामाजिक इतिहास, आम इन्सान का चरित्र, आचार-व्यवहार, रीति-नीति, रिवाज-संस्कार, गाड़ी-सवारी, पहनावे-ओढ़ावे, निम्न और श्रेष्ठ क्रिया-प्रतिक्रियाओं को मैंने यथासंभव प्रामाणिक और यथावत् रखने की कोशिश की है। हाँ, यह सच है कि बहुजातीय-बहुभाषी, इस विशाल-विराट भारतवर्ष के अन्तःकरण में उतरने के दौरान मुझे अपार विस्मय भी हुआ है, अपनी कमअक्ली पर संकोच भी हुआ है। इसके बावजूद इस संदर्भ में अपना निजी खयाल जाहिर करते हए, अपनी आँखों-देखी जानकारी और किताबें पढ़ने की आदत का सदुपयोग ज़रूर किया है।
इस किताब में देशी-विदेशी, कुल मिलाकर करीब एक सौ चरित्रों का उल्लेख है, लेकिन विदेशी मैकमोहन और भारतीय भवानीशंकर के बारे में मुझे अलग से कुछ नहीं कहना है। अंग्रेज़ मात्र ही बेहद क्रूर और अत्याचारी होते हैं, जैसे यह धारणा गलत है, उसी तरह यह भी महज वहम है कि वे लोग ही हमारे एकमात्र त्राणकर्ता थे। मैकमोहन उस बिरादरी में शामिल थे, जो सरकारी अफसर होने के बावजूद श्वेतांग फिरंगियों के समाज से अलग-थलग, भारतीय संग-साथ वक़्त गुज़ारते रहे, क्योंकि उन लोगों में कट्टरता का उन्माद नहीं था। ऐसे लोग जिस देश और संगति में रहते-सहते थे, वहाँ के बाशिंदों को उनके स्वभाव और अभाव में पहचानने की कोशिश करते थे, ये लोग मन के दरवाजे पहले से ही बन्द रखकर, मिलने-मिलाने के संयोग पर क़ैद नहीं लगाते थे।
हमारे यहाँ जिन्हें भारतीय तत्वविद् कहते् हैं, वे लोग ऐसे तो नहीं थे, लेकिन इन्हीं लोगों के अथक प्रयासों से इस देश की नृत्यकला, राजनीति, किस्से-कहानी, इतिहास, पशु-पक्षी और लता-पौधों के बारे में किताबें और हवाले प्रकाशित होते रहते और ज्ञानोन्मेष के साथ-साथ, जब हम स्वदेश अपनी सभ्यता-संस्कृति के बारे में आग्रही हुए, तब ये ही सरो-सामान हमारे मददगार बने। विदेशों से मिशनरी, शायद इस इरादे से भेजे गये थे कि वे इस देश के अनपढ़ पिछड़ी जातियों को धर्म के नशे में सुलाए रखें, लेकिन अधिकांश मिशनरियों का धर्म था—जन-सेवा, जन-कल्याण। उन लोगों ने दूर-दराज के दुर्गम प्रदेशों में शायद अपनी समूची जिंदगी गुजार दी। इतिहास के पन्नों में शायद उनका नाम दर्ज न हो, फिर भी हम बखूबी जानते हैं कि ये लोग दीन-हीन आम इनसानों के कितने करीब थे। फादर ब्राउन भी ऐसे ही एक चरित्र हैं। वैसे इस किताब में विपरीत चित्र और चरित्र भी मौजूद हैं।
आप इतिहास-चेता लोग इस हकी़कत से भी बखूबी परिचित हैं कि अंग्रेजी शिक्षा की रोशनी में शुरू-शुरू में अनगिनत भारतीय विद्वानों की आँखें चुँधिया गईं थीं और वे लोग स्वधर्म को तिलांजलि देकर यीशु-भक्तों की मेहरबानी से इस उन्नत धर्म में दीक्षित होने के लिए बेचैन हो उठे। उन्हें एकदम से लगा, हिन्दू समाज बेहद दकियानूस और लकीर का फकीर है और हिन्दू धर्म अतिशय गँवारु और अनुदार है। ऐसे में युगसाधक श्री रामकृष्ण और हिन्दू श्रेष्ठ विद्यासागर अपने सक्रिय प्रयासों के जरिए इतिहास के इस महासर्वनाश को रोकने के लिए दीवार बनकर खड़े हो गए। उन लोगों ने यह साबित कर दिखाया की जाति की मुक्ति सनातन धर्म में ही निहित है। उसे नज़रअन्दाज़ करके भागखड़े होने से समस्या का समाधान हरगिज नहीं होगा। भवानी शंकर भी उस क़िस्म के भारतवासियों के प्रतिनिधि। पता नहीं हू-ब-हू उस फ्रेम में फिट हो पाया या नहीं, लेकिन काफी कुछ उसी नक़्श में ढला हो, इसका मैंने यथासाध्य खयाल रखा है।
बृजदुलारी के साथ भवानीशंकर का रिश्ता कहानी के तकाजे पर बुना गया है। इसके बावजूद जिन्हें यह बात भली लगी हो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि भवानीशंकर के लिए तथाकथित प्रेम की तेज़ धार में बह जाना संभव नहीं था, खासकर बृजदुलारी जैसी औरत के साथ। जो औरत अपनी जिंदगी में घाट-घाट पर अनगिनत क़ीमत चुकाते हुए सिर्फ तजुर्बे ही खरीदती रही हो, जिसका अन्य किसी मानवीय अहसास से कभी कोई नाता-रिश्ता नहीं रहा, तो क्या उन दोनों के इर्द-गिर्द यह जो प्यार का वृत्त तैयार हो गया, वह क्या महज साजिश थी ? घटनाओं को ‘आइडियलाइज़्म’ करने के लिए ? नहीं ऐसा भी नहीं था। अनगिनत मर्दों की हमबिस्तर बृजदुलारी की देहयष्टि में उन्हें एक अदद शुद्ध-पवित्र दिल भी नज़र आया था और उन्हें लगा था कि उसकी रक्षा करना उनका फ़र्ज है। दरअसल प्यार से ज्यादा यह कर्तव्यबोध ही भवानीशंकर को बृजदुलारी के करीब ले आया था। अब यह बताना क्या ज़रूरी है कि सख़्त जिम्मेदारी और कर्तव्यपरायणता की भूरि-भूरि मिसाल तत्कालीन बंगाली समाज में मौजूद थी ?
नानासाहब ऐतिहासिक चरित्र हैं। मैंने अपनी निगाह सहज उनके गार्हस्थ जीवन तक ही सीमित रखी है। कानपुर हत्याकांड और युद्ध के परवर्ती पर्व में उनकी भूमिका बहस-मुबाहसे से परे आज भी मुझे विश्वसनीय नहीं लगती, इसलिए मैंने उन विवादास्पद प्रसंगों को नहीं छुआ है। मेरी राय में उम्र से अधेड़ यह संभ्रांत ब्राह्मण जंग के संकटकाल से भी पहले धन-दौलत, ज़मीन-जायदाद और पारिवारिक समस्याओं में फँसा हुआ था। अंग्रेजों द्वारा प्रचारित ‘Myth that is Nana’ और भारतीय जनमानस में ‘देशप्रेमी’, ‘श्रेष्ठ योद्धा-नाना’—इन दोनों ही परिचय की जड़ें अतिशय मज़बूत हैं और सालों से प्रचारित होने की वजह से अब सुप्रतिष्ठित हो चुकी हैं। ‘अमृत-संचय’ के नानासाहब, न तो friend of Cawnpore हैं, न ‘अमर-योद्धा’ ! उनके बारे में उपलब्ध तथ्यों के सहारे उनकी जो मूरत रची गई है, उसे देख-पढ़कर इतिहास में खिलौना बने इस अभागे को पाठक अगर अपना करीबी व्यक्ति मान सकें, तो मुझे लगेगा मेरी कोशिश सार्थक हुई।
आखिर में एक और बात कहना चाहूँगी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में कोई स्पष्ट राय आज तक उपलब्ध नहीं है। इतिहास के सिलसिले में भरपूर रोमांस या हर घटना के त्राहि-त्राहि चीत्कारं में ही हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। खुद मैंने भी यही कुछ नहीं किया, ऐसी बात भी नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है इतिहास-सृजन अतिरिक्त जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक ख़ास प्रवणता कहानी के बजाय—देश, काल, पात्र, रीति-रिवाज का विशेष ज्ञान बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा, आधुनिक चिंतन-मनन भी अनिवार्य है, क्योंकि इतिहास महज अतीत का ही आईना नहीं है, History is written precisely when the historian’s vision of the past is illuminated by insight into the problems of the present. यानी इतिहास-लेखन में अतीत के साथ-साथ, इतिहासकार की अंतर्दृष्टि, वर्तमान की समस्याओं के संदर्भ में भी रोशन हो और इतिहास भविष्य का पथ-निर्देशक भी तो है। नज़र आनेवाली घटनाओं की आड़ में इतिहास का रूपांतर अंदर ही अंदर लगातार जारी रहता है। इस उपन्यास में कोई ऐतिहासिक भूल-चूक या भ्रांति न हो, इसका मैंने यथासंभव ध्यान रखा है। लेकिन, अंग्रेज कूपर के हुक्म पर पंजाब में जो क़त्लेआम हुआ और सन् 1858 के बीच के महीनों में कानपुर में हुए हत्याकांड में महज साल-भर का फ़र्क़ था—उपन्यास के तकाज़े पर यह मैंने जानबूझकर लिखा है।
इसी उपन्यास में एक जगह मैंने ज़िक्र किया है—अंग्रेजी हुकूमत की पुनर्प्रतिष्ठा के बाद भी उनमें भारतीय गुप्तचर जिम्मेदार पदों पर विभूषित थे और उन लोगों ने ग्रामवासियों को ख़बर देकर, उनके फरार होने में मदद की थी। अन्यत्र, मैंने चंद अंग्रेज और आयरिश फौजियों का जिक्र किया है, जो भारतीय लोगों की तरफ से लड़े थे। ये दोनों घटनाएँ जिन लोगों को अविश्वसनीय लगें, उनकी जानकारी के लिए मेरा निवेदन है कि इतिहास में भी इस हक़ीकत का समर्थन मिलता है और अगर वे लोग चाहें, तो मोर टॉमसन, फ्रेडरिक कूपर, सर हिउग्राफ और रीस की किताबें जरूर पढ़ लें। इससे पहले मासिक ‘बसुमति’ पत्रिका (बाँगला) में इस उपन्यास का एक नौसिखुआ और स्वतंत्र रूप धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। उस बारे में स्वभावतः ही आज मुझे संकोच हो रहा है। ‘अमृत संचय’ मैंने तीन सालों के दौरान अलग-अलग समय में लिखा है; जिंदगी की अनगिनत आफत-विपदाओं के बावजूद ! साल-भर पहले यह उपन्यास पूरा हुआ है। बदलते हुए वक्त के साथ, ज्ञान और तजुर्बे भी बदलते रहे। मैं चाहती हूँ, इस दौरान जो दोष-त्रुटियाँ मेरी निगाहों को अचानक बेहद बड़ी लगी हैं, उन्हें सुधार दूँ। लेकिन, अगले ही पल मुझे यह भी लगा है कि इन्सान की इच्छाओं का कोई अन्त नहीं। किसी भी लेखक को भरपूर संतोष कभी नहीं होता, शायद होना भी नहीं चाहिए।
विशाल भारत का सामग्रिक रूप, लगभग लुप्तप्राय। तमाम प्रदेश अलग-अलग द्वीपों में बँटे-बिखरे; आत्मकेंद्रित ! आम इनसान ज्यादातर अपने-अपने में मगन। अशिक्षा और कुसंस्कारों ने उन्हें दास बना डाला था। दूसरी तरफ क्षमता का लोभ, धन-दौलत की प्रचुरता और इन्हीं के बीच हिंदू-मुसलमान और आंग्ल समाज की पँचमेल सभ्यता का शोरगुल। इसी संधिस्थल से यह उपन्यास शुरू होता है। और तैंतीस साल बाद उस बिन्दु पर खत्म होता है, जहाँ भारतीय जनमानस के चेहरे और विन्यास में परिवर्तन का आभास नज़र आने लगा। जहाँ व्यक्ति-चेतना और सोच-विचार में शिक्षा का प्रभाव स्पष्ट आकार लेने लगा था।
सन् सत्तावन में अंग्रेजों की हुकूमत। उन दिनों भारत के दो-तिहाई हिस्सों में जो विराट अभ्युत्थान करवट ले रहा था, उसकी गति-विकृति के बारे में आज भी मतविरोध है। किसी-किसी की राय इसे ‘पहला स्वतंत्रता संग्राम’ या ‘राष्ट्रीय विद्रोह’ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय विरोध, राष्ट्रीय विद्रोह के सुपरिचित लक्षण, इनका अभीष्ट लक्ष्य और संघर्ष के तरीकों में समानता का अभाव था। उन लोगों की नज़र में यह एक ‘आपात घटना’ या ‘Immediate event’ थी।
दूसरी तरफ इसे ‘आपात घटना’ न मानते हुए, कई-कई इतिहासकारों की राय में फौजी विक्षोभ का कारण किसान वर्ग के जीवन में निहित था, जो कर्ज़ से जर्जर और गरीबी की मार से बदहाल थे। इसे ‘Civil rebellion’ नाम देकर, इस विद्रोह को समाज के विभिन्न स्तरों पर छिड़े विभिन्न विक्षोभों के साथ जोड़कर, इनमें एक योगसूत्र क़ायम करने की कोशिश की गई। इन इतिहासकारों का शायद यह खयाल है कि सिपाहियों के उस शोषण की वजह से भारतीय जनमानस में परिचित तजुर्बों की बुनियाद हिल गई और उस दिन से शिक्षित समाज के मन में भी ब्रिटिश शासन के प्रति विद्वेष गहराने लगा। बाद में वही राष्ट्रीय संग्राम की नवीनतम पटभूमि के सृजन का सूत्रधार बना। नील विद्रोह, प्रेस एक्ट और एलबर्ट बिल वगैरह के जरिए प्रत्यक्ष न सही, अप्रत्यक्ष रूप से शायद वही लालसा ही फलीभूत हुई। सन् 1857 के आन्दोलन में बंगालियों की कोई भूमिका क्यों नहीं थी, इस बारे में भी कई-कई मतविरोध हैं। बहरहाल, वजह चाहे जो भी हो, यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उस ज़माने में बंगाली समुदाय अगर इस विद्रोह में भागीदार होता भी तो अंग्रेज़ी शासन का आकस्मिक अवसान नामुमकिन था और बाद के वक्तों में शिक्षा, शिल्प, ज्ञान साहित्य के क्षेत्र में और स्वस्थ, सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अप्रतिबद्ध वर्ग के तौर पर बंगाल का जबर्दस्त आत्मप्रकाश, भारतीय इतिहास को इस क़दर जटिल, विचित्र और अमोघ नहीं बना पाता।
मैंने उपन्यास में भारतवर्ष के उस संकटकाल और संसूचित नव-चेतना के समय को सफल साबित करने की कोशिश की है। उपन्यास लिखते हुए किसी सुनिश्चित कहानी की ज़रूरत होती है। लेकिन उस कहानी को छोड़ दें, तो उस युग के भारतवर्ष का राजनीतिक-सामाजिक इतिहास, आम इन्सान का चरित्र, आचार-व्यवहार, रीति-नीति, रिवाज-संस्कार, गाड़ी-सवारी, पहनावे-ओढ़ावे, निम्न और श्रेष्ठ क्रिया-प्रतिक्रियाओं को मैंने यथासंभव प्रामाणिक और यथावत् रखने की कोशिश की है। हाँ, यह सच है कि बहुजातीय-बहुभाषी, इस विशाल-विराट भारतवर्ष के अन्तःकरण में उतरने के दौरान मुझे अपार विस्मय भी हुआ है, अपनी कमअक्ली पर संकोच भी हुआ है। इसके बावजूद इस संदर्भ में अपना निजी खयाल जाहिर करते हए, अपनी आँखों-देखी जानकारी और किताबें पढ़ने की आदत का सदुपयोग ज़रूर किया है।
इस किताब में देशी-विदेशी, कुल मिलाकर करीब एक सौ चरित्रों का उल्लेख है, लेकिन विदेशी मैकमोहन और भारतीय भवानीशंकर के बारे में मुझे अलग से कुछ नहीं कहना है। अंग्रेज़ मात्र ही बेहद क्रूर और अत्याचारी होते हैं, जैसे यह धारणा गलत है, उसी तरह यह भी महज वहम है कि वे लोग ही हमारे एकमात्र त्राणकर्ता थे। मैकमोहन उस बिरादरी में शामिल थे, जो सरकारी अफसर होने के बावजूद श्वेतांग फिरंगियों के समाज से अलग-थलग, भारतीय संग-साथ वक़्त गुज़ारते रहे, क्योंकि उन लोगों में कट्टरता का उन्माद नहीं था। ऐसे लोग जिस देश और संगति में रहते-सहते थे, वहाँ के बाशिंदों को उनके स्वभाव और अभाव में पहचानने की कोशिश करते थे, ये लोग मन के दरवाजे पहले से ही बन्द रखकर, मिलने-मिलाने के संयोग पर क़ैद नहीं लगाते थे।
हमारे यहाँ जिन्हें भारतीय तत्वविद् कहते् हैं, वे लोग ऐसे तो नहीं थे, लेकिन इन्हीं लोगों के अथक प्रयासों से इस देश की नृत्यकला, राजनीति, किस्से-कहानी, इतिहास, पशु-पक्षी और लता-पौधों के बारे में किताबें और हवाले प्रकाशित होते रहते और ज्ञानोन्मेष के साथ-साथ, जब हम स्वदेश अपनी सभ्यता-संस्कृति के बारे में आग्रही हुए, तब ये ही सरो-सामान हमारे मददगार बने। विदेशों से मिशनरी, शायद इस इरादे से भेजे गये थे कि वे इस देश के अनपढ़ पिछड़ी जातियों को धर्म के नशे में सुलाए रखें, लेकिन अधिकांश मिशनरियों का धर्म था—जन-सेवा, जन-कल्याण। उन लोगों ने दूर-दराज के दुर्गम प्रदेशों में शायद अपनी समूची जिंदगी गुजार दी। इतिहास के पन्नों में शायद उनका नाम दर्ज न हो, फिर भी हम बखूबी जानते हैं कि ये लोग दीन-हीन आम इनसानों के कितने करीब थे। फादर ब्राउन भी ऐसे ही एक चरित्र हैं। वैसे इस किताब में विपरीत चित्र और चरित्र भी मौजूद हैं।
आप इतिहास-चेता लोग इस हकी़कत से भी बखूबी परिचित हैं कि अंग्रेजी शिक्षा की रोशनी में शुरू-शुरू में अनगिनत भारतीय विद्वानों की आँखें चुँधिया गईं थीं और वे लोग स्वधर्म को तिलांजलि देकर यीशु-भक्तों की मेहरबानी से इस उन्नत धर्म में दीक्षित होने के लिए बेचैन हो उठे। उन्हें एकदम से लगा, हिन्दू समाज बेहद दकियानूस और लकीर का फकीर है और हिन्दू धर्म अतिशय गँवारु और अनुदार है। ऐसे में युगसाधक श्री रामकृष्ण और हिन्दू श्रेष्ठ विद्यासागर अपने सक्रिय प्रयासों के जरिए इतिहास के इस महासर्वनाश को रोकने के लिए दीवार बनकर खड़े हो गए। उन लोगों ने यह साबित कर दिखाया की जाति की मुक्ति सनातन धर्म में ही निहित है। उसे नज़रअन्दाज़ करके भागखड़े होने से समस्या का समाधान हरगिज नहीं होगा। भवानी शंकर भी उस क़िस्म के भारतवासियों के प्रतिनिधि। पता नहीं हू-ब-हू उस फ्रेम में फिट हो पाया या नहीं, लेकिन काफी कुछ उसी नक़्श में ढला हो, इसका मैंने यथासाध्य खयाल रखा है।
बृजदुलारी के साथ भवानीशंकर का रिश्ता कहानी के तकाजे पर बुना गया है। इसके बावजूद जिन्हें यह बात भली लगी हो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि भवानीशंकर के लिए तथाकथित प्रेम की तेज़ धार में बह जाना संभव नहीं था, खासकर बृजदुलारी जैसी औरत के साथ। जो औरत अपनी जिंदगी में घाट-घाट पर अनगिनत क़ीमत चुकाते हुए सिर्फ तजुर्बे ही खरीदती रही हो, जिसका अन्य किसी मानवीय अहसास से कभी कोई नाता-रिश्ता नहीं रहा, तो क्या उन दोनों के इर्द-गिर्द यह जो प्यार का वृत्त तैयार हो गया, वह क्या महज साजिश थी ? घटनाओं को ‘आइडियलाइज़्म’ करने के लिए ? नहीं ऐसा भी नहीं था। अनगिनत मर्दों की हमबिस्तर बृजदुलारी की देहयष्टि में उन्हें एक अदद शुद्ध-पवित्र दिल भी नज़र आया था और उन्हें लगा था कि उसकी रक्षा करना उनका फ़र्ज है। दरअसल प्यार से ज्यादा यह कर्तव्यबोध ही भवानीशंकर को बृजदुलारी के करीब ले आया था। अब यह बताना क्या ज़रूरी है कि सख़्त जिम्मेदारी और कर्तव्यपरायणता की भूरि-भूरि मिसाल तत्कालीन बंगाली समाज में मौजूद थी ?
नानासाहब ऐतिहासिक चरित्र हैं। मैंने अपनी निगाह सहज उनके गार्हस्थ जीवन तक ही सीमित रखी है। कानपुर हत्याकांड और युद्ध के परवर्ती पर्व में उनकी भूमिका बहस-मुबाहसे से परे आज भी मुझे विश्वसनीय नहीं लगती, इसलिए मैंने उन विवादास्पद प्रसंगों को नहीं छुआ है। मेरी राय में उम्र से अधेड़ यह संभ्रांत ब्राह्मण जंग के संकटकाल से भी पहले धन-दौलत, ज़मीन-जायदाद और पारिवारिक समस्याओं में फँसा हुआ था। अंग्रेजों द्वारा प्रचारित ‘Myth that is Nana’ और भारतीय जनमानस में ‘देशप्रेमी’, ‘श्रेष्ठ योद्धा-नाना’—इन दोनों ही परिचय की जड़ें अतिशय मज़बूत हैं और सालों से प्रचारित होने की वजह से अब सुप्रतिष्ठित हो चुकी हैं। ‘अमृत-संचय’ के नानासाहब, न तो friend of Cawnpore हैं, न ‘अमर-योद्धा’ ! उनके बारे में उपलब्ध तथ्यों के सहारे उनकी जो मूरत रची गई है, उसे देख-पढ़कर इतिहास में खिलौना बने इस अभागे को पाठक अगर अपना करीबी व्यक्ति मान सकें, तो मुझे लगेगा मेरी कोशिश सार्थक हुई।
आखिर में एक और बात कहना चाहूँगी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, ऐतिहासिक उपन्यास के बारे में कोई स्पष्ट राय आज तक उपलब्ध नहीं है। इतिहास के सिलसिले में भरपूर रोमांस या हर घटना के त्राहि-त्राहि चीत्कारं में ही हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। खुद मैंने भी यही कुछ नहीं किया, ऐसी बात भी नहीं। लेकिन अब मुझे लगता है इतिहास-सृजन अतिरिक्त जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक ख़ास प्रवणता कहानी के बजाय—देश, काल, पात्र, रीति-रिवाज का विशेष ज्ञान बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा, आधुनिक चिंतन-मनन भी अनिवार्य है, क्योंकि इतिहास महज अतीत का ही आईना नहीं है, History is written precisely when the historian’s vision of the past is illuminated by insight into the problems of the present. यानी इतिहास-लेखन में अतीत के साथ-साथ, इतिहासकार की अंतर्दृष्टि, वर्तमान की समस्याओं के संदर्भ में भी रोशन हो और इतिहास भविष्य का पथ-निर्देशक भी तो है। नज़र आनेवाली घटनाओं की आड़ में इतिहास का रूपांतर अंदर ही अंदर लगातार जारी रहता है। इस उपन्यास में कोई ऐतिहासिक भूल-चूक या भ्रांति न हो, इसका मैंने यथासंभव ध्यान रखा है। लेकिन, अंग्रेज कूपर के हुक्म पर पंजाब में जो क़त्लेआम हुआ और सन् 1858 के बीच के महीनों में कानपुर में हुए हत्याकांड में महज साल-भर का फ़र्क़ था—उपन्यास के तकाज़े पर यह मैंने जानबूझकर लिखा है।
इसी उपन्यास में एक जगह मैंने ज़िक्र किया है—अंग्रेजी हुकूमत की पुनर्प्रतिष्ठा के बाद भी उनमें भारतीय गुप्तचर जिम्मेदार पदों पर विभूषित थे और उन लोगों ने ग्रामवासियों को ख़बर देकर, उनके फरार होने में मदद की थी। अन्यत्र, मैंने चंद अंग्रेज और आयरिश फौजियों का जिक्र किया है, जो भारतीय लोगों की तरफ से लड़े थे। ये दोनों घटनाएँ जिन लोगों को अविश्वसनीय लगें, उनकी जानकारी के लिए मेरा निवेदन है कि इतिहास में भी इस हक़ीकत का समर्थन मिलता है और अगर वे लोग चाहें, तो मोर टॉमसन, फ्रेडरिक कूपर, सर हिउग्राफ और रीस की किताबें जरूर पढ़ लें। इससे पहले मासिक ‘बसुमति’ पत्रिका (बाँगला) में इस उपन्यास का एक नौसिखुआ और स्वतंत्र रूप धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। उस बारे में स्वभावतः ही आज मुझे संकोच हो रहा है। ‘अमृत संचय’ मैंने तीन सालों के दौरान अलग-अलग समय में लिखा है; जिंदगी की अनगिनत आफत-विपदाओं के बावजूद ! साल-भर पहले यह उपन्यास पूरा हुआ है। बदलते हुए वक्त के साथ, ज्ञान और तजुर्बे भी बदलते रहे। मैं चाहती हूँ, इस दौरान जो दोष-त्रुटियाँ मेरी निगाहों को अचानक बेहद बड़ी लगी हैं, उन्हें सुधार दूँ। लेकिन, अगले ही पल मुझे यह भी लगा है कि इन्सान की इच्छाओं का कोई अन्त नहीं। किसी भी लेखक को भरपूर संतोष कभी नहीं होता, शायद होना भी नहीं चाहिए।
महाश्वेता देवी
1
सन् 1857 की जनवरी की एक शाम !
कानपुर के क़रीब बिठूर रियासत ! एक वृहद प्रासाद के दूसरे तल पर एक विशाल कक्ष में, कोई अधेड़-से ब्राह्मण आरामकुर्सी पर विराजमान। रंग सांवला। स्थूलकाय चेहरे पर हजामत के दाग़। सिर घुटा हुआ। नुकीली नाक। पतले और दबे हुए से होंठ। सिर पर बेशक़ीमती पगड़ी। कान और गले में मोतियों के कुण्डल और माला ! उनकी एक बाँह अलस भाव से आराम कुर्सी के हत्थे पर पड़ी हुई है। दूसरे हाथ में हुक्के की नली। लेकिन नली उनके होंठों पर नहीं थी। हुक्के से सुगंधित तँबाकू की भीनी-भीनी खुशबू आती है। दूसरी हथेली रह-रहकर, जब हिलती-डुलती है, उस पर आतिशदान की रोशनी झलमला उठती है। उनकी तर्जनी, मध्यमा, अनामिका तीनों उँगलियों में नवरत्न, मूँगा, मोती हीरे-पन्ने की कई-कई अँगूठियाँ। ये अँगूठियाँ सिर्फ अलंकार ही नहीं थीं, शायद ग्रह,-नक्षत्रों की शान्ति के लिए धारण की गई थीं। बदन पर ढीला-ढाला ऊनी कुर्ता। गले में पड़े हुए सुनहरे जनेऊ का सिरा नज़र आता हुआ। उनकी आँखें बेहद गंभीर और थकी-थकी सी। उम्र चालीस से ज़रा ऊपर।
कोई वृद्ध ब्राह्मण, उनके करीब ही खड़े, उनसे बातचीत में मग्न। वे भी दीर्घकाय, गौरवर्ण, मुंडितकेश ! पूस की कड़कड़ाती ठंड में भी उनके बदन पर सिर्फ ऊनी उत्तरी। पाँवों में खड़ाऊँ। वे खड़े-खड़े ही बातें करते रहे। बीच-बीच में तीखी-उजली निगाहों से अपनी दाहिनी हथेली भी निहारे जा रहे थे। बातचीत का तरीका भी बेहद धीर-गंभीर। मानो छंदबद्ध लहजे में कोई पत्र पढ़कर सुना रहे थे। उनके खड़े होने की भंगिमा थी बेहद शांत-संयत ! आवाज़ कसी हुई। इसके बावजूद उनके लहजे में कैसा तो उद्धत स्पर्द्धा का भाव, मानों सामने वाले शख़्स को सम्मान देने का उन्हें कोई चाव नहीं, न ही वे उनकी श्रेष्ठता या पद-मर्यादा क़बूल करने को राजी हैं।
सामनेवाले शख़्स थे—नाना धोंदूपंत ! स्वर्गीय बाजीराव के द्वितीय के दत्तक पुत्र और उनके मनोनीत उत्तरा अधिकारी। दूसरे व्यक्ति थे—विश्वेश्वर मंगल थाट्टे। नाना के पिता तुल्य, स्वर्गीय चिमनाजी अप्पा के पोते, चिमना जी थाटे के पितृकुल के पुरोहित। असंख्य मामलों में नाना की दोनों सौतेली माताओं, सौतेली बहनो-योगबाई और कुसुमबाई से उनकी तकरार छिड़ी रहती थी। योग और कुसुम के मामा बलवंत अटवाले चाहते थे कि उनकी भानजियों को ज़मीन-जायदाद में बराबरी का हिस्सा मिले। नाना कि विमाताएँ सारी धन-दौलत, चोरी-चोरी चिमनाजी थाट्टे को सौंप देने को बैचैन थीं। विश्वेश्वर मंगल थाट्टे उनके अतिशय विश्वासपात्र थे। वे बेहद आचारनिष्ठ, कूटनीतिज्ञ और तेजस्वी ब्राह्मण थे।
अंतःपुर की यह दुरभिसंधि, नाना की हवेली में अशांति के बीज बो गई थी। बाहर भी उनकी जान को चैन नहीं था। वे बेहद शांतिप्रिय और निरीह इनसान थे। लेकिन खानदानी ज़र-ज़मीन, धन-दौलत उनके गले की फाँस बन गई थी और उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। विश्वेश्वर मंगल थाट्टे, नाना साहब के पास कोई आवेदन लेकर आए थे। उनकी भृकुटि रह-रहकर खिड़की की तरफ उठ जाती थी। जबरदस्त सर्दी के बावजूद, खिड़की खुली हुई थी। बाहर पूस की शाम का धूसरआसमान नज़र आता हुआ। खिड़की के ठीक नीचे, कोई बाज़ीगर, बैठा-बैठा पटाखों का तमाशा दिखा रहा था। बीच-बीच में रंगीन अनार की रोशनी उछल-उछल कर खिड़की के ऊपर तक झाँक जाती थी। उस चकाचौंध रोशनी में कमरे में जलता हुआ आतिशदान निष्प्रभ लग रहा था।
विश्वेश्वर को लगा, महत्त्वपूर्ण बातचीत के दौरान रोशनी का यह महोत्सव, मानो बाधा खड़ी कर रहा है। उसकी निगाह पेशवा पर लगी हुई थी लेकिन वे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उन्हें मालूम था यह बाज़ीगर पेशवा का विशेष स्नेहभाजन था। उन्हें यह भी पता था कि आज उनके आमंत्रण पर जो अंग्रेज साहब कानपुर से बिठूर तशरीफ लाए थे, उन्हीं के दिल बहलाव के लिए बाज़ीगर को ख़बर भेजी गई थी। यह बाज़ीगर पिछले दस सालों से बूढ़ें बाज़ीराव और नाना धुंधूपंथ से कितनी दौलत ऐंठ चुका है ! उन्होंने मन-ही-मन हिसाब लगाने की कोशिश की।
बुजुर्ग बाजीराव की स्वजन-प्रीति खासी गहरी थी। दक्षिण के जितने सारे महाराष्ट्री ब्रह्मावर्त उनकी शरण में आए थे, बाजीराव उन लोगों को अपना आश्रित मानते थे। असंख्य लोगों के साथ इस अधेड़ बाज़ीगर के पुरखे पेशवा साम्राज्य के विगत गौरव के दौर में पूना, सतारा, रायगढ़ और कोलाबा में पटाखों का तमासा दिखाने आया करते थे। बाजीराव प्रथम के एक-एक विजय-गौरव के मौके पर छत्रपति शाहू जब जश्न मनाने का हुक्म जारी करते, ये लोग बेहतरीन पटाखे तैयार करके रोशनी का त्योहार मनाते। अपने गाँव कौकन में इन लोगों ने प्रचुर ज़मीन-ज़ायदाद जमा कर ली।
विश्वेश्वर का खयाल था, उन दिनों इस क़िश्म के ज़श्न की सार्थकता भी थी। उस जमाने में पेशवा लोगों ने मध्य-भारत की एक-एक रियासत-बड़ोदरा, बीजापुर वगैरह जीतकर, अपनी दखल में ले लिया था और राजकोष में बेशुमार दौलत का भंडार जमा होता रहा। होल्कर, गायकवाड़ और सिंधिया लोग सिर झुकाए-झुकाए पेशवाओं के हुक्म बजा लाते।
विश्वेश्वर मन ही मन बुदबुदा उठे, ‘उन दिनों यह, आलकोत्सव पेशवाओं की विजयलक्ष्मी का अभिनंनदन करता था। आज ये लोग चंद अंग्रेजों को खुश करने के लिए जश्न का आयोजन करने में लगे थे।
पेशवा उनके मन का असंतोष भांप गए।
मुँह फेरने के बजाय उन्होंने अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट की, ‘‘अंग्रेज साहब पटाखों का जलवा देखना चाहते हैं। अगर उसका तमाशा पसंद आ गया, तो उसे कानपुर बुला भेजेंगे। उसे रेजिमेंट के स्पोर्ट्स के मौके पर तमाशा दिखाने जाना होगा। उसका बेटा अफसोस कर रहा था, इन दिनों उसे कोई नहीं बुलाता।’’
विश्वेश्वर किंचित् अचकचा गए।
उन्होंने अपना आवेदन दोबारा पेश किया, ‘‘आपकी दोनों माताश्री परेशान हैं। आपके पिताश्री के गंगालाभ पर, आपने पंच महादान जो नहीं किया।’’
‘ऐसी बात तो नहीं है। मैंने हाथी-घोड़ा, सोना-चाँदी और रत्न तो दान किया था। मैंने अपना सबसे बेहतरीन हाथी भी दान दे दिया। घुड़साल के लिए मैंने चुने हुए अरबी घोड़े खरीदे थे, उनमें से घोड़ा भी दान कर दिया। इसके अलावा दान में सिर्फ सोना ही नहीं, मोती-मूँगा, गोमेद-पन्ना वगैरह नौ रत्न भी दिए थे। हाँ, ज़मीन मेरे पास इंच भर नहीं थी। वह तो रघुनाथ राव विष्णुरकर ही था, जिसने अपनी सारी जागीर और ईनाम में मिली सारी ज़मीन पूरे के पूरे बावन गाँव ही मुझे अर्पित करना चाहा, उस वक्त, उस स्वामिभक्त सरदार की बातें सुनकर मेरी आँखें भीग आईं...’ नाना किसी सोच में डूब गए, ‘‘लेकिन मैंने उनका दान नहीं लिया। किसी और से ज़मीन लेकर दिए गए दान से स्वर्ग में बैठे मेरे पिता की आत्मा को हरगिज शांति नहीं मिलती। इसके अलावा, जो ज़मीन एक बार दान कर दी गई, उसे वापस लेना मेरे लिए असंभव था।’’
इतना कहकर नाना खामोस हो गए। उनकी आवाज़ बेहद सर्द और उदास लगी।
विश्वेश्वर ने जवाब दिया, ‘‘इसीलिए आपकी दोनों माताश्री ने प्रस्ताव भेजा है कि तक़दीर अगर आपसे नाराज है, तो बिठोबा, महालक्ष्मी और गणेश इन तीनों देवताओं को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए। इसीलिए...’
‘‘अभी पिछले ही दिनों तो माताओं ने यज्ञ आयोजित किया था। मेरे लखनऊ से लौटने के फौरन बाद ही तो पूजा शुरू हुई थी।’’
‘वह तो आपकी खातिर; पुत्र-कामना के लिए...’
विश्वेश्वर की आवाज़ भावलेशहीन थी। नाना का साँवला चेहरा, धीरे-धीरे लाल हो उठा। इन दिनों उनकी विमाताओं को शक हो गया था कि उनमें बेटा पैदा करने की क्षमता नहीं है। तभी तो उन्हें इस कदर नीचा दिखाती रहती हैं।
बहरहाल, उन्होंने बातचीत जारी रखी, ‘पेशवा वंश कहीं खत्म न हो जाए, इसकी फिक्र मुझे भी है। लेकिन मेरा खयाल है अभी तत्काल यज्ञ-हवन, पूजा-पाठ की जरूरत नहीं है। मेरी कनिष्ठिका पत्नी काशीबाई अभी बालिका है...’
बेहद धीर और स्पष्ट शब्दों में विश्वेश्वर ने जवाब दिया, ‘आपको अपनी मातृ-द्वय की ममता पर संशय हो रहा है ? श्रीमान, उन्हें साफ़ नज़र आने लगा है कि विलायत में आपकी अर्जी मंजूर कर दी गई है। उनकी आँखें यह भी देख रही हैं कि अपने स्वर्गीय पिता की सील-मुहर का उपयोग करने की अनुमति भी आपको नहीं मिली। वे लोग ठहरी औरत जात ! उनका चित्त सहज ही व्याकुल हो उठा है।’
तभी तो उन लोगों ने अपना-अपना वकील भेजकर रेजीडेंट साहब के दरबार में अपनी फरियाद पहुँचाई और अभी कल तक ज़मीन-जायदाद को लेकर अंतःपुर में भीषण तूफान मचा रहा।
नाना साहब ने पूछा, ‘‘अब क्या करना होगा ?’’
‘‘गंगा तट पर अनुष्ठान ! नौचंडी पाठ ! और गंगाजल में भिगोकर सोने-चाँदी की मुद्रा-दान ! यह सब तत्काल ज़रूरी है, श्रीमान् ! उन्होंने आपको सूचित करने को कहा है।’’
विश्वेश्वर खामोश हो गए।
कानपुर के क़रीब बिठूर रियासत ! एक वृहद प्रासाद के दूसरे तल पर एक विशाल कक्ष में, कोई अधेड़-से ब्राह्मण आरामकुर्सी पर विराजमान। रंग सांवला। स्थूलकाय चेहरे पर हजामत के दाग़। सिर घुटा हुआ। नुकीली नाक। पतले और दबे हुए से होंठ। सिर पर बेशक़ीमती पगड़ी। कान और गले में मोतियों के कुण्डल और माला ! उनकी एक बाँह अलस भाव से आराम कुर्सी के हत्थे पर पड़ी हुई है। दूसरे हाथ में हुक्के की नली। लेकिन नली उनके होंठों पर नहीं थी। हुक्के से सुगंधित तँबाकू की भीनी-भीनी खुशबू आती है। दूसरी हथेली रह-रहकर, जब हिलती-डुलती है, उस पर आतिशदान की रोशनी झलमला उठती है। उनकी तर्जनी, मध्यमा, अनामिका तीनों उँगलियों में नवरत्न, मूँगा, मोती हीरे-पन्ने की कई-कई अँगूठियाँ। ये अँगूठियाँ सिर्फ अलंकार ही नहीं थीं, शायद ग्रह,-नक्षत्रों की शान्ति के लिए धारण की गई थीं। बदन पर ढीला-ढाला ऊनी कुर्ता। गले में पड़े हुए सुनहरे जनेऊ का सिरा नज़र आता हुआ। उनकी आँखें बेहद गंभीर और थकी-थकी सी। उम्र चालीस से ज़रा ऊपर।
कोई वृद्ध ब्राह्मण, उनके करीब ही खड़े, उनसे बातचीत में मग्न। वे भी दीर्घकाय, गौरवर्ण, मुंडितकेश ! पूस की कड़कड़ाती ठंड में भी उनके बदन पर सिर्फ ऊनी उत्तरी। पाँवों में खड़ाऊँ। वे खड़े-खड़े ही बातें करते रहे। बीच-बीच में तीखी-उजली निगाहों से अपनी दाहिनी हथेली भी निहारे जा रहे थे। बातचीत का तरीका भी बेहद धीर-गंभीर। मानो छंदबद्ध लहजे में कोई पत्र पढ़कर सुना रहे थे। उनके खड़े होने की भंगिमा थी बेहद शांत-संयत ! आवाज़ कसी हुई। इसके बावजूद उनके लहजे में कैसा तो उद्धत स्पर्द्धा का भाव, मानों सामने वाले शख़्स को सम्मान देने का उन्हें कोई चाव नहीं, न ही वे उनकी श्रेष्ठता या पद-मर्यादा क़बूल करने को राजी हैं।
सामनेवाले शख़्स थे—नाना धोंदूपंत ! स्वर्गीय बाजीराव के द्वितीय के दत्तक पुत्र और उनके मनोनीत उत्तरा अधिकारी। दूसरे व्यक्ति थे—विश्वेश्वर मंगल थाट्टे। नाना के पिता तुल्य, स्वर्गीय चिमनाजी अप्पा के पोते, चिमना जी थाटे के पितृकुल के पुरोहित। असंख्य मामलों में नाना की दोनों सौतेली माताओं, सौतेली बहनो-योगबाई और कुसुमबाई से उनकी तकरार छिड़ी रहती थी। योग और कुसुम के मामा बलवंत अटवाले चाहते थे कि उनकी भानजियों को ज़मीन-जायदाद में बराबरी का हिस्सा मिले। नाना कि विमाताएँ सारी धन-दौलत, चोरी-चोरी चिमनाजी थाट्टे को सौंप देने को बैचैन थीं। विश्वेश्वर मंगल थाट्टे उनके अतिशय विश्वासपात्र थे। वे बेहद आचारनिष्ठ, कूटनीतिज्ञ और तेजस्वी ब्राह्मण थे।
अंतःपुर की यह दुरभिसंधि, नाना की हवेली में अशांति के बीज बो गई थी। बाहर भी उनकी जान को चैन नहीं था। वे बेहद शांतिप्रिय और निरीह इनसान थे। लेकिन खानदानी ज़र-ज़मीन, धन-दौलत उनके गले की फाँस बन गई थी और उन्हें लगातार परेशान कर रही थी। विश्वेश्वर मंगल थाट्टे, नाना साहब के पास कोई आवेदन लेकर आए थे। उनकी भृकुटि रह-रहकर खिड़की की तरफ उठ जाती थी। जबरदस्त सर्दी के बावजूद, खिड़की खुली हुई थी। बाहर पूस की शाम का धूसरआसमान नज़र आता हुआ। खिड़की के ठीक नीचे, कोई बाज़ीगर, बैठा-बैठा पटाखों का तमाशा दिखा रहा था। बीच-बीच में रंगीन अनार की रोशनी उछल-उछल कर खिड़की के ऊपर तक झाँक जाती थी। उस चकाचौंध रोशनी में कमरे में जलता हुआ आतिशदान निष्प्रभ लग रहा था।
विश्वेश्वर को लगा, महत्त्वपूर्ण बातचीत के दौरान रोशनी का यह महोत्सव, मानो बाधा खड़ी कर रहा है। उसकी निगाह पेशवा पर लगी हुई थी लेकिन वे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि उन्हें मालूम था यह बाज़ीगर पेशवा का विशेष स्नेहभाजन था। उन्हें यह भी पता था कि आज उनके आमंत्रण पर जो अंग्रेज साहब कानपुर से बिठूर तशरीफ लाए थे, उन्हीं के दिल बहलाव के लिए बाज़ीगर को ख़बर भेजी गई थी। यह बाज़ीगर पिछले दस सालों से बूढ़ें बाज़ीराव और नाना धुंधूपंथ से कितनी दौलत ऐंठ चुका है ! उन्होंने मन-ही-मन हिसाब लगाने की कोशिश की।
बुजुर्ग बाजीराव की स्वजन-प्रीति खासी गहरी थी। दक्षिण के जितने सारे महाराष्ट्री ब्रह्मावर्त उनकी शरण में आए थे, बाजीराव उन लोगों को अपना आश्रित मानते थे। असंख्य लोगों के साथ इस अधेड़ बाज़ीगर के पुरखे पेशवा साम्राज्य के विगत गौरव के दौर में पूना, सतारा, रायगढ़ और कोलाबा में पटाखों का तमासा दिखाने आया करते थे। बाजीराव प्रथम के एक-एक विजय-गौरव के मौके पर छत्रपति शाहू जब जश्न मनाने का हुक्म जारी करते, ये लोग बेहतरीन पटाखे तैयार करके रोशनी का त्योहार मनाते। अपने गाँव कौकन में इन लोगों ने प्रचुर ज़मीन-ज़ायदाद जमा कर ली।
विश्वेश्वर का खयाल था, उन दिनों इस क़िश्म के ज़श्न की सार्थकता भी थी। उस जमाने में पेशवा लोगों ने मध्य-भारत की एक-एक रियासत-बड़ोदरा, बीजापुर वगैरह जीतकर, अपनी दखल में ले लिया था और राजकोष में बेशुमार दौलत का भंडार जमा होता रहा। होल्कर, गायकवाड़ और सिंधिया लोग सिर झुकाए-झुकाए पेशवाओं के हुक्म बजा लाते।
विश्वेश्वर मन ही मन बुदबुदा उठे, ‘उन दिनों यह, आलकोत्सव पेशवाओं की विजयलक्ष्मी का अभिनंनदन करता था। आज ये लोग चंद अंग्रेजों को खुश करने के लिए जश्न का आयोजन करने में लगे थे।
पेशवा उनके मन का असंतोष भांप गए।
मुँह फेरने के बजाय उन्होंने अपनी तरफ से स्थिति स्पष्ट की, ‘‘अंग्रेज साहब पटाखों का जलवा देखना चाहते हैं। अगर उसका तमाशा पसंद आ गया, तो उसे कानपुर बुला भेजेंगे। उसे रेजिमेंट के स्पोर्ट्स के मौके पर तमाशा दिखाने जाना होगा। उसका बेटा अफसोस कर रहा था, इन दिनों उसे कोई नहीं बुलाता।’’
विश्वेश्वर किंचित् अचकचा गए।
उन्होंने अपना आवेदन दोबारा पेश किया, ‘‘आपकी दोनों माताश्री परेशान हैं। आपके पिताश्री के गंगालाभ पर, आपने पंच महादान जो नहीं किया।’’
‘ऐसी बात तो नहीं है। मैंने हाथी-घोड़ा, सोना-चाँदी और रत्न तो दान किया था। मैंने अपना सबसे बेहतरीन हाथी भी दान दे दिया। घुड़साल के लिए मैंने चुने हुए अरबी घोड़े खरीदे थे, उनमें से घोड़ा भी दान कर दिया। इसके अलावा दान में सिर्फ सोना ही नहीं, मोती-मूँगा, गोमेद-पन्ना वगैरह नौ रत्न भी दिए थे। हाँ, ज़मीन मेरे पास इंच भर नहीं थी। वह तो रघुनाथ राव विष्णुरकर ही था, जिसने अपनी सारी जागीर और ईनाम में मिली सारी ज़मीन पूरे के पूरे बावन गाँव ही मुझे अर्पित करना चाहा, उस वक्त, उस स्वामिभक्त सरदार की बातें सुनकर मेरी आँखें भीग आईं...’ नाना किसी सोच में डूब गए, ‘‘लेकिन मैंने उनका दान नहीं लिया। किसी और से ज़मीन लेकर दिए गए दान से स्वर्ग में बैठे मेरे पिता की आत्मा को हरगिज शांति नहीं मिलती। इसके अलावा, जो ज़मीन एक बार दान कर दी गई, उसे वापस लेना मेरे लिए असंभव था।’’
इतना कहकर नाना खामोस हो गए। उनकी आवाज़ बेहद सर्द और उदास लगी।
विश्वेश्वर ने जवाब दिया, ‘‘इसीलिए आपकी दोनों माताश्री ने प्रस्ताव भेजा है कि तक़दीर अगर आपसे नाराज है, तो बिठोबा, महालक्ष्मी और गणेश इन तीनों देवताओं को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए। इसीलिए...’
‘‘अभी पिछले ही दिनों तो माताओं ने यज्ञ आयोजित किया था। मेरे लखनऊ से लौटने के फौरन बाद ही तो पूजा शुरू हुई थी।’’
‘वह तो आपकी खातिर; पुत्र-कामना के लिए...’
विश्वेश्वर की आवाज़ भावलेशहीन थी। नाना का साँवला चेहरा, धीरे-धीरे लाल हो उठा। इन दिनों उनकी विमाताओं को शक हो गया था कि उनमें बेटा पैदा करने की क्षमता नहीं है। तभी तो उन्हें इस कदर नीचा दिखाती रहती हैं।
बहरहाल, उन्होंने बातचीत जारी रखी, ‘पेशवा वंश कहीं खत्म न हो जाए, इसकी फिक्र मुझे भी है। लेकिन मेरा खयाल है अभी तत्काल यज्ञ-हवन, पूजा-पाठ की जरूरत नहीं है। मेरी कनिष्ठिका पत्नी काशीबाई अभी बालिका है...’
बेहद धीर और स्पष्ट शब्दों में विश्वेश्वर ने जवाब दिया, ‘आपको अपनी मातृ-द्वय की ममता पर संशय हो रहा है ? श्रीमान, उन्हें साफ़ नज़र आने लगा है कि विलायत में आपकी अर्जी मंजूर कर दी गई है। उनकी आँखें यह भी देख रही हैं कि अपने स्वर्गीय पिता की सील-मुहर का उपयोग करने की अनुमति भी आपको नहीं मिली। वे लोग ठहरी औरत जात ! उनका चित्त सहज ही व्याकुल हो उठा है।’
तभी तो उन लोगों ने अपना-अपना वकील भेजकर रेजीडेंट साहब के दरबार में अपनी फरियाद पहुँचाई और अभी कल तक ज़मीन-जायदाद को लेकर अंतःपुर में भीषण तूफान मचा रहा।
नाना साहब ने पूछा, ‘‘अब क्या करना होगा ?’’
‘‘गंगा तट पर अनुष्ठान ! नौचंडी पाठ ! और गंगाजल में भिगोकर सोने-चाँदी की मुद्रा-दान ! यह सब तत्काल ज़रूरी है, श्रीमान् ! उन्होंने आपको सूचित करने को कहा है।’’
विश्वेश्वर खामोश हो गए।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i